- Post by Admin on Tuesday, Jun 03, 2025
- 803 Viewed

डॉ. राजाराम त्रिपाठी: एक बार फिर पाँच जून आ पहुँचा है। यानी वह दिन जब हम “विश्व पर्यावरण दिवस” के नाम पर बड़ी श्रद्धा से एक बार फिर सारी घिसी-पिटी औपचारिकताएँ निभाएँगे। कोई बरगद का बोंजाई गमले में लगाएगा, तो कोई नौतपा में पीपल, जामुन ,आम के पौधे लगाएगा, कोई हरे-भरे गमले थामे हुए सेल्फी खिंचवाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम की दीवारें ‘ग्रीन अर्थ, क्लीन अर्थ’ जैसे नारों से पट जाएँगी। अधिकारीगण भाषण देंगे, कुछ भाषण सुनने की रस्म निभाएँगे। और अगले दिन सब अपने-अपने निर्धारित एजेंडे पर लौट जाएँगे।यानी पर्यावरण-विनाश की एकसूत्रीय योजना में पुनः सक्रिय हो जाएँगे।
दरअसल, हमने कभी पर्यावरण की चिंता की ही नहीं। हमारा विकास मॉडल ही ऐसा है जिसमें प्रकृति के लिए कोई स्थान ही नहीं। विज्ञान से हमने क्या सीखा? यही कि हर प्रगति अब प्रकृति पर एक और प्रहार है। हमने विज्ञान को विकास का औजार तो बना लिया, पर विवेक को कूड़ेदान में डाल दिया। परिणाम यह कि विकास और पर्यावरण अब एक वाक्य में दो तलवारों की तरह हो गए हैं—जो एक म्यान में साथ रह ही नहीं सकते। आज जलवायु परिवर्तन केवल एक वैश्विक बहस नहीं, हमारे फेफड़ों में घुला जहर बन चुका है।
कहीं तापमान 50 डिग्री पार कर गया है, तो कहीं बर्फ़बारी जून में हो रही है। लगता है, पृथ्वी अपने संतुलन को खो चुकी है—कभी आग बरसाती गर्मी, तो कभी “आइस एज” की आहट। भारत में इस वर्ष मई 2024 में राजस्थान के फालौदी में तापमान 50.5°C दर्ज किया गया—जो भारत में अब तक का सर्वाधिक तापमान बन गया। इसी वर्ष दिल्ली में 29 मई तापमान 49.9°C रहा। बादल अब मौसम विभाग की परिभाषाओं को ठेंगा दिखाते हैं। न कैलेंडर में दर्ज ऋतुएँ समय पर आती हैं, न पंचांगों के ग्रह नक्षत्र अब वर्षा का अनुमान दे पाते हैं।
IPCC की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पिछले 50 वर्षों में मानसून की स्थिरता 27% तक घट गई है। 'प्रतीक्षित वर्षा' और 'वास्तविक वर्षा' के बीच का अंतर अब औसतन 19% हो गया है। पर हमारे विकास मॉडल को देखिए—वह सस्टेनेबिलिटी से कोसों दूर भागता है। अब पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हम बड़े गर्व से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं। *मानो बिजली से चलने वाला वाहन अपने आप में समस्त पर्यावरण पापों को विनष्ट करने वाला 'पावन गंगा जल' हो गया हो!* परन्तु क्या कभी हमने आत्मा से पूछ कर देखा है कि उस बैटरी के निर्माण और निष्पादन की प्रक्रिया कितनी विषैली है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार भारत में 2022-23 में लगभग 70,000 टन लिथियम-आयन बैटरियाँ आयात हुईं, जिनमें से 95% का कोई पर्यावरण-सुरक्षित रीसायक्लिंग सिस्टम नहीं है।
उनकी रीसायक्लिंग की प्रक्रिया या तो अस्तित्व में नहीं है या बेहद सीमित है। दूसरा सवाल—वह बिजली कहाँ से आ रही है जिससे ये पर्यावरण हितैषी का ठप्पा माथे पर चिपकाए हमारी ये ईवी चार्ज होते हैं? क्या कोयले से बिजली बनाना प्रदूषण मुक्त प्रक्रिया है? भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में 72% से अधिक हिस्सा आज भी थर्मल पावर प्लांट्स का है। इनमें से अधिकांश कोयले से चलने वाले हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और फ्लाई ऐश का प्रमुख स्रोत हैं। (स्रोत: CEA - Central Electricity Authority, 2024) और *जिस सौर ऊर्जा को हम 'पवित्र गाय' मान बैठे हैं,* क्या उसकी सोलर प्लेट्स को हम 100% रीसायकल कर सकते हैं? फ्रेंच एनवायर्नमेंटल एजेंसी (ADEME) की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सोलर पैनल का केवल 10-15% ही प्रभावी रूप से रीसायकल हो रहा है।
भारत में यह प्रतिशत और भी कम है। आज खेतों में करोड़ों टन रासायनिक खाद डाली जा रही है, जिसकी गैसें जल, थल, नभ तीनों को बर्बाद कर रही हैं। कीटनाशकों से न केवल मिट्टी मर रही है, बल्कि वह ‘मृत्युभोज’ धीरे-धीरे हमारे शरीर में पहुँच रहा है। FAO (Food and Agriculture Organization) की रिपोर्ट (2022) के अनुसार, भारत की 30% कृषि भूमि मध्यम से लेकर गंभीर रूप से मिट्टी-प्रदूषण की शिकार है। पर्यावरण की इस दुर्दशा में अकेले व्यक्ति नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी समान रूप से दोषी हैं—या कहें कि उनके पास ‘अधिकांश अधिकार’ सुरक्षित हैं। उनके उत्पाद, उनके ब्रांड, उनके हित—सब पर्यावरण की कीमत पर सुरक्षित हैं। और कई सरकारें तो उनके इशारे पर ही कार्य करती प्रतीत होती हैं।
अब सोचिए, क्या सचमुच हम इस नीले ग्रह को रहने योग्य बनाए रखना चाहते हैं? अथवा इससे भी बड़ा सवाल—क्या हम, मनुष्य जाति, इस पृथ्वी पर रहने योग्य प्राणी हैं? आपने कभी सुना कि किसी बकरी, किसी शेर, किसी तेंदुए ने किसी वनस्पति या प्राणी प्रजाति को नष्ट कर दिया हो? नहीं। यह कारनामा केवल मनुष्य कर सकता है। वह विकास के नाम पर जंगलों की हत्या करता है, जैवविविधता का संहार करता है, और फिर खुद को ‘सभ्य’ कहता है। यूनाइटेड नेशंस बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट (2020) के अनुसार, मानव गतिविधियों के कारण प्रतिदिन लगभग 150 प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं।
आज हम चंद्रमा पर पहुँचने की खुशी में उछल रहे हैं, मंगल पर ‘बस्ती बसाने’ के ख्वाब पाल रहे हैं। पर ज़रा सोचिए—अगर पृथ्वी, जहाँ ऑक्सीजन निशुल्क है, जल लगभग सहज उपलब्ध है, जहाँ प्रकृति अपने दम पर हर वर्षा ऋतु में जल, जीवन ,बनस्पति जगत के पुनर्जीवन का प्रयास करती है, अगर हमारे ही कुकर्मों के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं रहा, तो प्रयोगशालाओं में बनाई गई ऑक्सीजन, पानी और पौधे के सहारे चाँद-मंगल पर कितने लोग, कितने दिन जिंदा रह पाएँगे? विज्ञान को नकारना समाधान नहीं, पर विवेकहीन विज्ञान अनिष्ट ही करता है।
मानवता का संरक्षण यदि हमारा उद्देश्य है तो सबसे पहले हमें इस पृथ्वी को संरक्षित करना होगा। ‘रहने योग्य ग्रह’ की खोज से पहले ‘रहने योग्य समाज’ का निर्माण करना ज़रूरी है। यही कारण है कि हमें अब विकसित समाज के अहंकार से बाहर निकल कर आदिवासी समाज की ओर देखना होगा। वे, जो हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ सहजीवन में रहकर सिखाते आए हैं कि "विकास" केवल ऊँची इमारतों का नाम नहीं, बल्कि धरती व प्रकृति के साथ संतुलित सहजीवन का नाम है। हम जिन्हें “पिछड़ा आदिवासी” कहते हैं, वे हमें दिखाते हैं कि कैसे बिना प्लास्टिक के, बिना जहर के खेती की जा सकती है। कैसे जल का सम्मान किया जा सकता है, कैसे वनों के साथ जीते हुए भी वनों की रक्षा की जा सकती है। ‘मिश्रित खेती’, बचे-खुचे ‘परंपरागत बीज’, ‘वनस्पतिजन्य दुर्लभ औषधियाँ’—इन सबका ज्ञान इन जनजातियों के पास है, जिन्हें हमने विकास की दौड़ में तिलांजलि दे दी थी। किंतु हमें “शिक्षक” नहीं, “शिष्य” बनकर इन जनजातीय ज्ञान परंपराओं के पास जाना होगा।
तभी हम इस पृथ्वी को सचमुच बचा पाएँगे। अंत में...विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक तारीख नहीं, एक गंभीर चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि अगली पीढ़ी को केवल विरासत में मोबाइल और मेट्रो नहीं, पीने का पानी, सांस लेने की हवा और टिकाऊ जीवन प्रणाली भी चाहिए। आज की वैज्ञानिक दृष्टि को ऋषि-दृष्टि के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारे पूर्वज कह गए हैं: *"पृथिव्यां त्रायते यः स धर्मः" — जो पृथ्वी की रक्षा करे वही धर्म है।* और याद रखिए—"यस्य किञ्चिद्ज्ञानं स विनश्यति" — जिसने थोड़ा-सा भी ज्ञान पाया, पर विवेक खो बैठा, उसका विनाश निश्चित है।इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि ‘हम पृथ्वी को कैसे बचाएँ’, बल्कि यह भी है—क्या हम खुद को बचा पाने योग्य बना पाए हैं?

अन्य समाचार

अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष 2025 : वरिष्ठ साहित्यकार दीनदयाल साहू को 24 भाषाओं और 70 आदिवासी समुदायों के लेखकों के बीच छत्तीसगढ़ी कहानी वाचन के लिए आमंत्रित किया गया
देश–विदेश से आए कथाकारों, उपन्यासकारों और शोधार्थियों के बीच इस तीन दिवसीय महोत्सव में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला भिलाई नगर निवासी वरिष्ठ साहित्यकार और संपादक दीनदयाल साहू को
Read More...
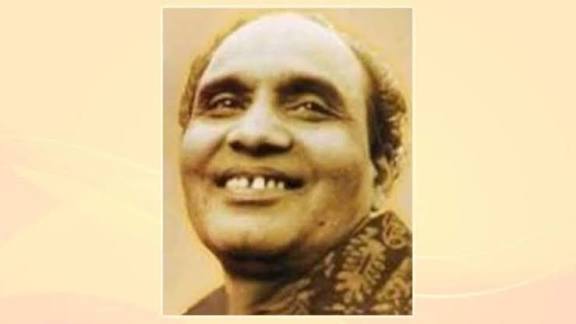
सत्यदर्शन साहित्य : भरी-पूरी हों सभी बोलियां,यही कामना हिंदी है...गहरी हो पहचान आपसी,यही साधना हिंदी है...गिरिजाकुमार माथुर
गिरिजाकुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर (मध्यप्रदेश) में हुआ था। वे आधुनिक हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे
Read More...
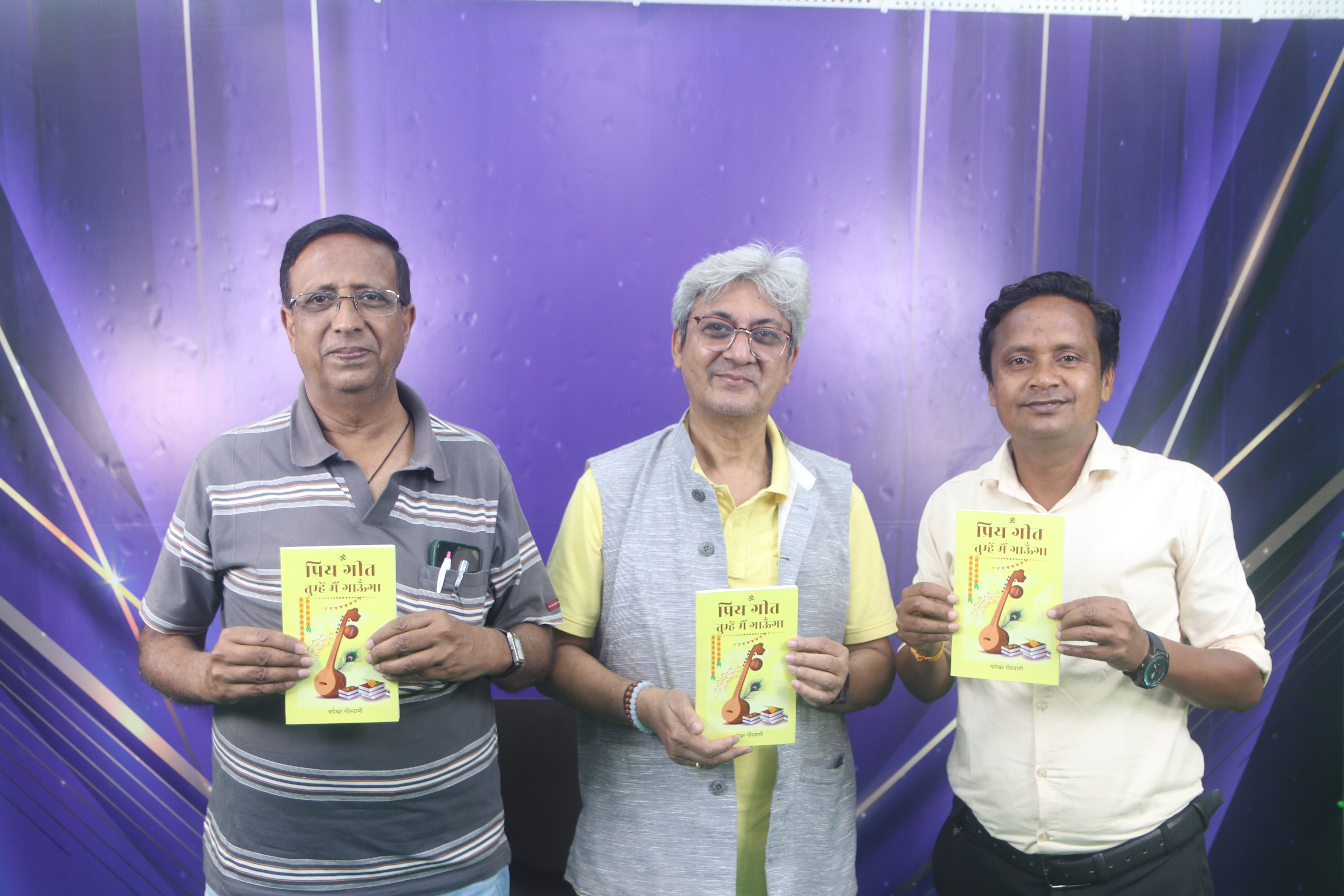
सत्यदर्शन साहित्य... प्रिय गीत तुम्हें मैं गाऊंगा : छत्तीसगढ़ की आत्मा से जुड़ा गीत-संग्रह
छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गीतकार चम्पेश्वर गोस्वामी द्वारा रचित गीत-संग्रह “प्रिय गीत तुम्हें मैं गाऊंगा” साहित्य और संगीत की दुनिया में एक नई पहचान बना रहा है।
Read More...
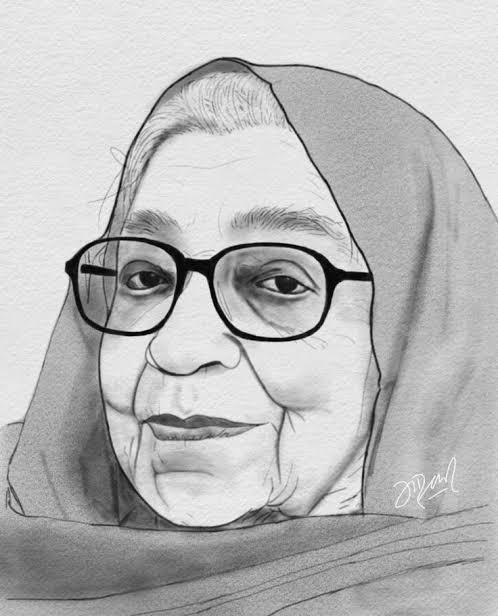
जो तुम आ जाते एक बार....महादेवी वर्मा
महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका और समाजसेविका थीं, जिन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। वे छायावादी काव्य धारा की चार प्रमुख स्तंभों में से एक थीं। उनकी कविताओं में गहन करुणा, संवेदनशीलता और आध्यात्मिक प्रेम की झलक मिलती है।
Read More...

लोक संस्कृति के अमर राग: 69 वर्षीय दुर्वासा कुमार टण्डन को मानद डॉक्टरेट उपाधि
69 वर्षीय प्रसिद्ध लोक कलाकार दुर्वासा कुमार टण्डन ने यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन, निरंतर साधना और संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम उम्र की सीमाओं को लांघ सकता है।
Read More...

आत्मचिंतन : धरती पर जब पहली बार मानव ने आँख खोली थी, तब उसके हाथ में न मोबाइल था, न मशीन! बस एक बीज था और आकाश में टकटकी लगाए विश्वास की दृष्टि
वे वृक्षों को अपना कुल-गोत्र कहते हैं, हर पशु पक्षी में अपना पूर्वज ढूँढ़ते हैं, और हर नदी में माँ का आशीष। पर विडंबना यह कि हम, स्वयं को 'सभ्य' कहने वाले, उसी धरती और जंगल को बेचकर अपनी तरक्की के महल खड़े कर रहे हैं।
Read More...
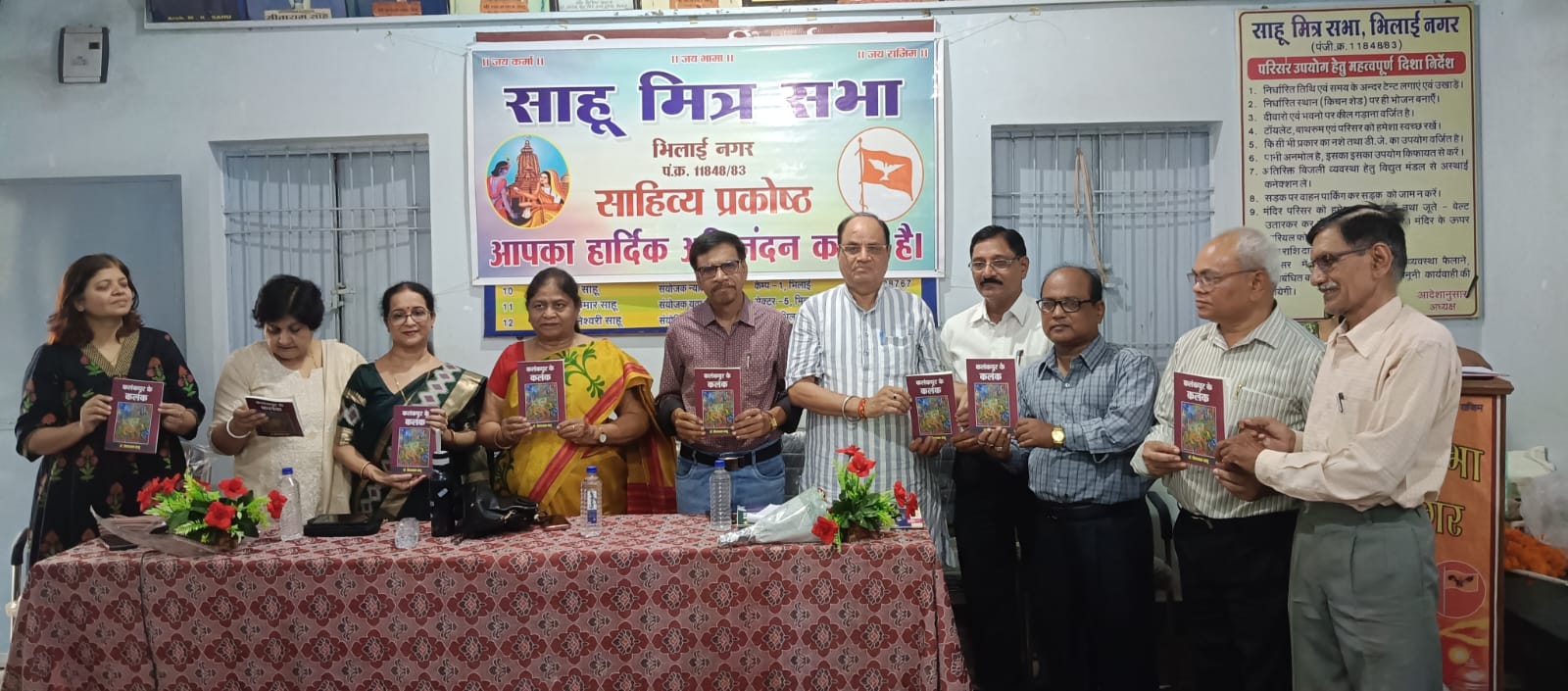
साहित्य और संवेदना का संगम : छत्तीसगढ़ी व्यंग्य साहित्य को समर्पित भव्य आयोजन
छत्तीसगढ़ी व्यंग्य संग्रह ‘कलंकपुर के कलंक’ का विमोचन, पर्यावरण संरक्षण के तहत वृक्षारोपण और सांस्कृतिक सौंध से सुवासित काव्य गोष्ठी सम्पन्न हुई।
Read More...

सावन...जब पेड़ हरियाली ओढ़ लेते हैं, नदियाँ गीत गाने लगती हैं और मन भी भीग जाता है
लघुकथा : गांव के छोटे से खेत में रहने वाला बालक अर्जुन, हर दिन की तरह उस दिन भी सुबह जल्दी उठ गया। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी।
Read More...

किसान की हरियाली को कागज़ी बंदिशों में मत घुटने दो
हर बार जब सरकार कोई नया कानून लाती है और कहती है कि यह “किसानों के हित में” है, तभी किसान का मन किसी अघोषित आपातकाल की तरह कांप उठता है
Read More...

हर बूंद में उम्मीद, हर बादल में कहानी और हर गरज में साहस ढूँढने की जरूरत
बारिश की रिमझिम बूंदें केवल मौसम को नहीं भिगोतीं, बल्कि हमारे मन-मस्तिष्क को भी प्रभावित करती हैं।
Read More...


